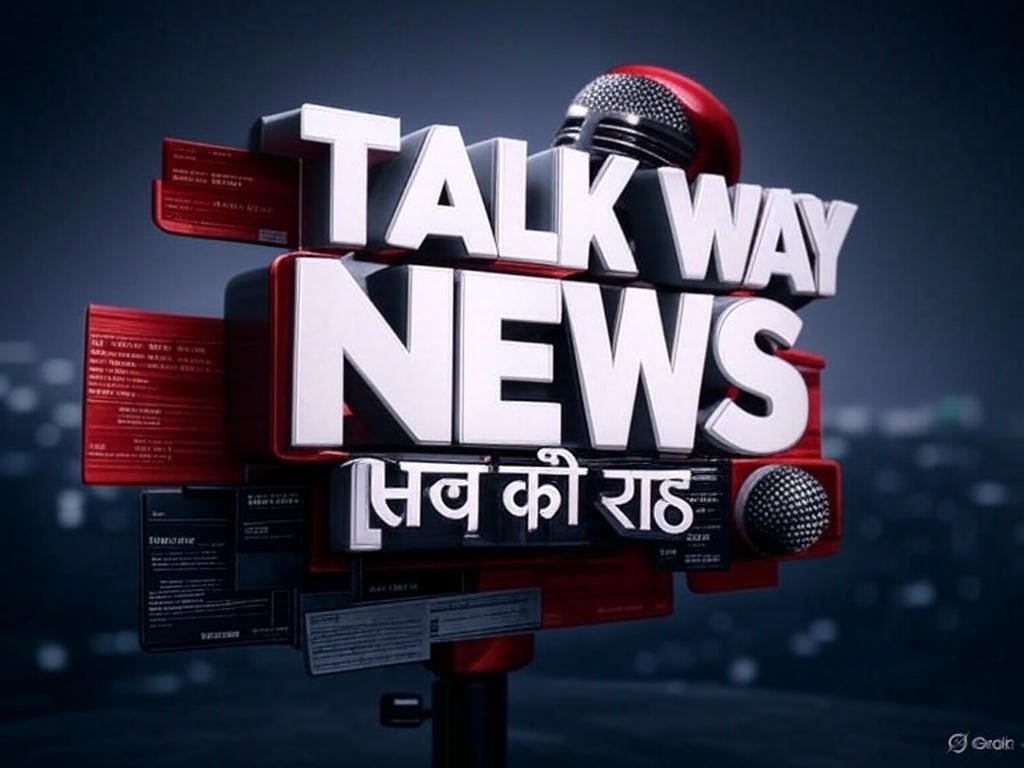नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता: अमित शाह बोले- अबूझमाड़ नक्सल मुक्त, दो दिन में 258 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण
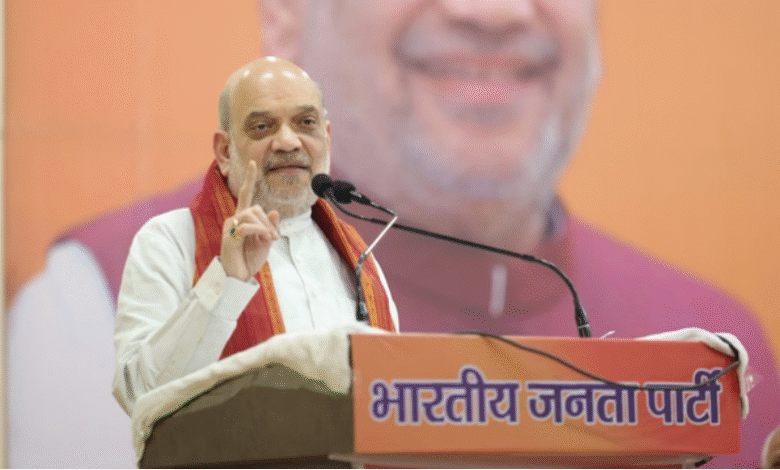
“अबूझमाड़ नक्सल मुक्त, दो दिन में 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया”
“नक्सलवाद” यानी वामपंथी उग्रवाद भारत के कुछ हिस्सों में दशकों से एक जटिल और संवेदनशील समस्या रही है। यह आंदोलन गरीबी, वंचना, आदिवासी जनसंख्या, सीमांत विकास, सरकार और सुरक्षा बलों की रणनीति और नक्सलियों के वैचारिक आग्रह — इन सभी जटिल कारणों से जुड़ा रहा है।
इस पृष्ठभूमि में, यदि कोई घोषणा होती है कि एक क्षेत्र “नक्सल मुक्त” हो गया है, या बड़े पैमाने पर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो यह घोषणा न केवल राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्ता रखती है, बल्कि उसकी सच्चाई, व्यावहारिक असर और चुनौतियाँ भी गहराई से जाँची जानी चाहिए।
घटना का कथित विवरण
-
घोषणा एवं आत्मसमर्पण की संख्या
-
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ (Abujhmad / अबूझमाड़) तथा उत्तरी बस्तर (North Bastar) इलाकों को नक्सल आतंक से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।
-
उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों में कुल 258 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं।
-
इनमें से 170 आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में हुए।
-
-
-
सरकार की रणनीति व नीति
-
अमित शाह व छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि यह सफलता “मोदी सरकार की नीति” और “नक्सलवाद उन्मूलन की प्रतिबद्धता” का परिणाम है।यह दावा किया गया कि पिछले जनवरी 2024 से अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर इलाकों में सुरक्षा, सशस्त्र अभियानों, विकास योजनाओं और जनभागीदारी के कारण स्थिति में सुधार हुआ है
-
यह भी कहा गया कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घट चुकी है, तथा “अत्यधिक प्रभावित जिलों” की सूची में भी कमी आई है।
-
भविष्य की समय-सीमा
-
सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ तथा अन्य प्रभावित इलाकों से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए।
-
विवाद एवं आलोचनाएँ
जब सरकार या नेता ऐसी बड़ी सफलताओं की घोषणा करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि इसके पीछे कुछ बहसें होंगी: वास्तविकता की सीमाएँ, राजनीतिक उद्देश्य, जनभावनाएँ, सुरक्षा चुनौतियाँ आदि। नीचे ऐसे कुछ प्रमुख विवाद-बिंदु:
-
विभिन्न “मुक्त” का अर्थ और दायरा
-
“नक्सल-मुक्त” कहने का मतलब यह हो सकता है कि अबूझमाड़ में सक्रिय नक्सली अभियान, अड्डे, हथियारबंद हिंसा न हो रही हो। लेकिन क्या पूरी तरह से उन सभी नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स, तस्करी, भर्ती आदि बंद हो गए हैं, यह कहना अभी मुश्किल है।
-
कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि “South Bastar” में अभी भी नक्सल गतिविधियाँ जारी हैं। अर्थात् मुक्ति अभी पूर्ण नहीं; क्षेत्रीय अंतर मौजूद है।
-
-
आत्मसमर्पण की गुणवत्ता और सत्यापन
-
आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या यदि भारी-भरकम है, तो यह ज़रूरी है कि यह सत्यापित हो कि वे वास्तव में “कट्टर / battle-hardened” थे, और उनका नेटवर्क में कितना प्रभाव था।
-
क्या हथियारों की वापसी हुई है? क्या उनके पास हथियार थे? किस प्रकार के हथियार थे? मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ हद तक “हथियारों की जब्ती” की बात है, लेकिन हर आत्मसमर्पण के साथ हथियारों की मात्रा एवं प्रकार पर पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है।
-
-
राजनीतिक उद्देश्य / प्रचार तत्व
-
चुनावी चक्र, सरकार की सार्वजनिक छवि, विकास-मंत्रणा, नक्सल-मुक्त भारत की योजना आदि को ध्यान में रखकर ऐसी घोषणाएँ नीति-निर्माताओं को लाभ पहुंचाती हैं।
-
“31 मार्च 2026” की समय सीमा तय करना प्रभावी प्रतीत होता है, लेकिन इस तरह की समय सीमाएँ अक्सर प्रचार की रणनीति का हिस्सा होती हैं।
-
-
सुरक्षा एवं सामुदायिक चुनौतियाँ
-
जंगलों, दुर्गम इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों में कब्जा और प्रभाव स्थापित करना आसान नहीं। आत्मसमर्पण करने वालों की सुरक्षा, पुनर्वास और समुदाय में उनकी स्वीकार्यता की चुनौतियाँ होंगी।
-
नक्सलियों के पीछे अक्सर सामाजिक-आर्थिक कारक होते हैं — गरीबी, असमानता, आदिवासी आबादी का उपेक्षित होना, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी आदि। सिर्फ सुरक्षा अभियान और आत्मसमर्पण नीतियाँ पर्याप्त नहीं होतीं, यदि मूल कारणों को ठीक से न सुलझाया जाए।
-
-
विश्वसनीयता एवं पूर्व अनुभव
-
बीते वर्षों में कई ऐसी घोषणाएँ हुई हैं कि “नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम हुई है”, “नक्सलियों की ताकत दब- गई है” आदि, लेकिन अक्सर हिंसात्मक झड़पें, मृत्यु-घटनाएँ, पुनरुत्थान की घटनाएँ भी हुई हैं।
-
आत्मसमर्पण की संख्या बढ़ने से यह संकेत मिलता है कि नक्सल संगठन अस्थिरता की स्थिति में हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आंदोलन पूरी तरह खत्म हो गया हो।
-
राजनीतिक, सुरक्षा एवं सामुदायिक दृष्टिकोण
इस तरह की घटनाएँ विभिन्न हितधारकों (stakeholders) के लिए अलग-अलग मायने रखती हैं:
-
राजनीतिक दृष्टिकोण
-
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि की झण्डी है। चुनावी लाभ, जनता के बीच सरकार की साख बढ़ने की संभावना है।
-
BJP सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी/गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व को ऐसी सफलताओं से वैचारिक और रणनीतिक शक्ति मिलती है।
-
विपक्षी दलों के लिए यह मुद्दा होगा कि सरकार ने किन मानकों पर नक्सल-मुक्त घोषित किया, आत्मसमर्पण की वास्तविकता क्या है, और जनता को क्या लाभ मिला है।
-
-
सुरक्षा दृष्टिकोण
-
सुरक्षा बलों के सफल अभियानों, नियंत्रण-क्षमता, खुफिया जानकारी, जनभागीदारी और पुनर्वास/सुधार नीतियों का समन्वित प्रभाव इस सफलता के पीछे हो सकता है।
-
इससे नक्सलियों के अंदर भी भय/अविश्वास बढ़ेगा और नई भर्ती कम हो सकती है। हथियारों की जब्ती और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया से संगठन कमजोर होगा।
-
लेकिन, जंगलों में दुर्गम इलाकों में निगरानी, नियंत्रण, सुरक्षा दलों की तैनाती, घेराबंदी आदि लगातार बनी रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी “गैरसक्रिय आतंकवादी घटक” फिर से सक्रिय हो सकते हैं।
-
-
सामुदायिक दृष्टिकोण (स्थानीय लोग, जनजातियाँ, आदिवासी समुदाय)
-
आदिवासी इलाकों में जिन लोगों को भय, हिंसा, जैसी स्थितियाँ झेलनी पड़ी थीं, उनके लिए आत्मसमर्पण और “नक्सल-मुक्त” स्थिति एक नई आशा हो सकती है। स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क-पानी बिजली आदि विकास कार्यों की गति बढ़ सकती है।
-
लेकिन पुनर्समेकन (reintegration) चुनौती है: आत्मसमर्पण करने वालों को विश्वास दिलाना कि वे सुरक्षित होंगे, समाज में स्वीकार होंगे, उनकी आजीविका होगी। अक्सर पश्चात सामाजिक भेदभाव, पुलिस/सशस्त्र बलों द्वारा संदेह या उत्पीड़न की शिकायतें आती रही हैं।
-
स्थानीय समुदाय, आदिवासी नेतृत्व, नागरिक समाज NGO आदि की भागीदारी जरूरी है, ताकि विकास योजनाएँ उनकी ज़रूरतों के अनुरूप हों, जंगलों/भूमि अधिकारों की रक्षा हो, शिक्षा-स्वास्थ्य आदि सेवाएँ पहुँचें।
-
निष्कर्ष
इस तरह, “अबूझमाड़ नक्सलमुक्त” घोषणा एक बड़ी और महत्वाकांक्षी सफलता का प्रतीक है, जिसे सरकार और सुरक्षा बलों ने आत्मसमर्पण की संख्या, नीति-परिवर्तन और सक्रिय अभियानों के माध्यम से प्राप्त किया है। तथ्यों की जांच से यह स्पष्ट है कि अधिकांश रिपोर्ट्स एक दूसरे से सहमत हैं, आत्मसमर्पण और सरकारी निर्देशों के बीच कम अंतर है।
लेकिन यह कहना कि यह सफलता पूर्णतः सुरक्षित या स्थायी है, अभी असमर्थता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है:
-
“मुक्त” की स्थिति अस्थायी हो सकती है यदि सुरक्षा बलों की उपस्थिति, शासन-प्रक्रियाएँ और सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाएँ लगातार सक्रिय न हों।
-
आत्मसमर्पण करने वालों का पुनर्वास, आजीविका, समाज में पुनः संपर्क और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि पुनरुत्थान न हो।
-
आत्मसमर्पण की गुणवत्ता (उन व्यक्तियों की भूमिका, हथियारों की मात्रा व प्रकार) सार्वजनिक और पारदर्शी रूप से प्रस्तुत होनी चाहिए, ताकि जनता को सच्ची जानकारी मिले।
-
राजनीति के हितों से प्रेरित घोषणाएँ हो सकती हैं; इसलिए मीडिया, नागरिक समाज, मानवाधिकार संगठन इस प्रकार की घोषणाओं की निगरानी करें।
“सच्ची कहानी” — मेरी व्याख्या
अबूझमाड़-उत्तर बस्तर क्षेत्र वर्षों से नक्सलवाद के प्रभाव में रहा है: जंगलों की दुर्गमता, सीमित सरकारी पहुंच, आदिवासी आबादी के असंतोष, सीमित आधारभूत सुविधाएँ — इन सबने नक्सल आंदोलन को बढ़ावा दिया है। सुरक्षा बलों ने समय-समय पर अभियानों, अड्डों पर छापों, हथियार जब्त करने आदि के ज़रिए नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन अक्सर नक्सलियों का वापसी-मार्ग और पुनरुत्थान संभव रहा है।
2024 में जब भाजपा सरकार बनी, सरकार ने हमें प्रोत्साहनात्मक नीतियाँ और “स्वीकारोक्ति-नीति” (surrender policy), पुनर्वास एवं विकास योजनाएँ (roads, चेकपॉस्ट, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि) तेज़ की। साथ ही, सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया सूचनाएँ, स्थानीय आदिवासी नेताओं के साथ संवाद बढ़ने लगा। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया सरल करने की कोशिश हुई, आत्मसमर्पण की शर्तों में सुधार संभव हुआ।
16 अक्टूबर 2025 की घटना उस क्रम की परिणति है जिसमें 258 नक्सली दो दिनों में आत्मसमर्पण करते हैं — राज्य और केंद्र यह संकेत देना चाहते हैं कि अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर वह इलाके हैं जहाँ “हथियारबंद हिंसा” और “नक्सल नियंत्रण” की स्थिति अब खत्म हो गई है। यह एक मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक उपलब्धि है; जनता के बीच सरकार की पकड़ और विश्वास को बढ़ाएगा; आदिवासी इलाकों में विकास और शांति की उम्मीदों को जगाएगा।
लेकिन सच्चाई यह है कि “पूरी मुक्ति” तक पहुंचना आसान नहीं है। नक्सल आंदोलन जड़ों से जुदा नहीं है; सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, जंगलों का संबंध आदिवासी जीवन से, भूमि-अधिकार, न्याय और भरोसा जैसे मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। यदि आत्मसमर्पण करने वालों के जीवन-स्तर में सुधार नहीं हुआ, यदि सरकार की उपस्थिति स्थायी नहीं हुई, यदि स्थानीय सरकारों/पुलिस/सशस्त्र बलों में ज़्यादा पारदर्शिता और न्याय नहीं हुआ — तो स्थिति वापस उथलपुथल का शिकार हो सकती है।
-
-